क्षेत्रवाद: भारत की एकता में बाधा
विविधता में एकता भारत का आदर्श वाक्य रहा है, और इसे बनाए रखने के लिए, इस विचार को मजबूत करते हुए प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टता का जश्न मनाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास किए जाने चाहिए कि ये सभी क्षेत्र मिलकर एक एकल, अखंड भारत की जीवंत छवि बना सकें।
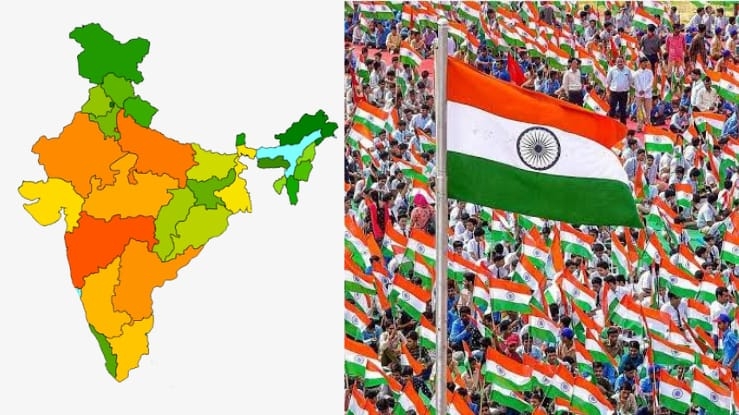
भारत अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध ऐसा देश हैं, जहाँ संस्कृतियों, भाषाओं, परंपराओं और विचारधाराओं का मिश्रण रहा है। हालाँकि यह विविधता निस्संदेह इसकी ताकतों में से एक है, लेकिन जब राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की बात आती है तो यह कुछ चुनौतियाँ भी उभर कर सामने आती है।
ऐसी ही एक चुनौती क्षेत्रवाद का उदय है, एक ऐसी घटना जहां लोगों की अपने विशिष्ट क्षेत्रों के प्रति निष्ठा और लगाव समग्र रूप से राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा पर हावी हो जाती है। जबकि क्षेत्रीय पहचान सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, अत्यधिक क्षेत्रवाद भारत की व्यापक एकता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। एकता में अनेकता के बोध पर क्षेत्रीयता का भाव बढ़ता जा रहा हैं।
भारत में क्षेत्रवाद कोई नई अवधारणा नहीं है; इसकी गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें हैं। देश के विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों को ऐतिहासिक कारकों, भाषाई मतभेदों और अनूठी परंपराओं द्वारा आकार दिया गया है।
इसके परिणामस्वरूप लोगों में अपने-अपने क्षेत्रों के प्रति लगाव और गर्व की स्वाभाविक भावना पैदा हुई है। लेकिन समस्याएं तब आती हैं, जब क्षेत्रवाद विभाजनकारी राजनीति के रूप में बदल जाता है या अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा देने लगता है। इन परिस्थितियों में क्षेत्रवाद, राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर चुनौती बन जाता है।
भारत में क्षेत्रवाद की बीज को पोषित करने का कार्य ब्रिटिशों के द्वारा किया गया। रियासतों के प्रति औपनिवेशिक नीतियों और व्यवहार ने उनके बीच क्षेत्रीयवादी प्रवृत्तियां विकसित की। ब्रिटिश शोषणकारी आर्थिक नीतियों ने कुछ क्षेत्रों की पूरी तरह से उपेक्षा की, जिससे आर्थिक असमानताओं और क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिला।
दूसरी ओर दक्षिणी भारत का बहुचर्चित द्रविड़ आंदोलन (1940) को क्षेत्रवाद आधारित आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। वर्तमान का गैर-ब्राह्मण आंदोलन का स्वरुप भी क्षेत्रवादी आंदोलन के समान ही है। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप एक अलग और स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग उठी। आंध्र क्षेत्र में एक अलग राज्य की मांग शुरू हुई।
भारत में क्षेत्रयिता आधारित राज्यों की मांग 1950 और 60 के दशक में बड़े पैमाने पर (हिंसक) लामबंदी देखी गई। पोट्टी श्री रामुलु ने सन 1954 में आंध्र के अलग राज्य के लिए विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी मृत्यु की घटना ने भारत में राजनीतिक क्षेत्रवाद की लहर शुरू कर दी। जिसका एक उदाहरण 2014 में आंध्र प्रदेश से विभाजित कर तेलंगाना राज्य का निर्माण है।
क्षेत्रवाद के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक इसकी संघर्षों को बढ़ावा देने और राष्ट्र के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने को बाधित करने की क्षमता है। जब विभिन्न क्षेत्रों को संसाधन आवंटन, विकास परियोजनाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, तो इससे एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा हो सकती है जो समग्र प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है।
इसके अलावा, जब क्षेत्रीय पहचान का उपयोग समुदायों का ध्रुवीकरण करने के लिए किया जाता है, तो यह नागरिकों के बीच कलह और अविश्वास के बीज बो सकता है। क्षेत्रीय पहचान का अभिन्न अंग होने के कारण भाषा एक विभाजनकारी मुद्दा भी बन सकती है। भारत की भाषाई विविधता विशाल है, प्रत्येक राज्य की अपनी आधिकारिक भाषा है।
हालाँकि भाषाई संरक्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे राष्ट्र को एकजुट करने वाली आम भाषा के महत्व पर हावी नहीं होना चाहिए। भाषा नीति पर बहस कभी-कभी संघर्ष में बदल जाती है, जिससे राष्ट्रीय संस्थानों के सुचारू कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है।
क्षेत्रवाद की बाधा को दूर करने के लिए, राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है जो क्षेत्रीय गौरव के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से मौजूद हो। शिक्षा इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह एकता के महत्व पर जोर देते हुए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की समझ को बढ़ावा दे सकती है।
सांस्कृतिक आदान-प्रदान, राष्ट्रीय त्योहारों और सहयोगी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने से विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के बीच अंतर को पाटने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, राजनीतिक नेताओं और पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वे अल्पकालिक लाभ के लिए क्षेत्रीय भावनाओं का फायदा उठाने से बचें।
इसके बजाय, उन्हें उन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो समान विकास को बढ़ावा देती हैं और सभी क्षेत्रों की चिंताओं का समाधान करती हैं। सत्ता का प्रभावी विकेंद्रीकरण राष्ट्र की व्यापक एकता को बनाए रखते हुए विशिष्ट क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय सरकारों को सशक्त बना सकता है।
क्षेत्रवाद के नकरात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर राज्यों द्वारा सामाजिक व्यय के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है जो मानव संसाधन विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। नीति आयोग का गठन बॉटम-अप दृष्टिकोण का उपयोग करके आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद को बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक कदम है।
जबकि समावेशी विकास के लिए सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की शुरूआत, पिछड़े राज्यों में विकास के लिए निजी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन जैसे कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन उनके प्रभावी कार्यान्वयन की अधिक आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक ऐसी प्रणाली शुरू करना चाहिए जो लोगों को क्षेत्रीय भावनाओं पर काबू पाने और राष्ट्रप्रेम विकसित करने में मदद करेगी, उप-राष्ट्रवाद की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के रूप में कार्य कर सकती है।
यदि किसी क्षेत्र के लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति पर वास्तविक गर्व है तो यह राष्ट्रीय एकता के लिए कोई समस्या नहीं हैं। क्षेत्रवाद किसी राष्ट्र के लिए समस्या या राष्ट्र-विरोधी घटना के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि यह अलगाववादी प्रवृत्तियों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उग्रवादी तथा आक्रामक स्थिति उत्पन्न हो।
क्षेत्रवाद, भारत के विविध सांस्कृतिक ताने-बाने में निहित होते हुए भी, चरम सीमा पर ले जाने पर इसकी एकता में बाधा बन सकता है। देश की समग्र प्रगति के लिए क्षेत्रीय गौरव और राष्ट्रीय निष्ठा के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।
समावेशी विकास को बढ़ावा देकर, साझा राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देकर और विभाजनकारी राजनीति को हतोत्साहित करके, भारत क्षेत्रवाद से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सकता है और एक एकजुट राष्ट्र के रूप में मजबूत होकर उभर सकता है।
विविधता में एकता भारत का आदर्श वाक्य रहा है, और इसे बनाए रखने के लिए, इस विचार को मजबूत करते हुए प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टता का जश्न मनाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास किए जाने चाहिए कि ये सभी क्षेत्र मिलकर एक एकल, अखंड भारत की जीवंत छवि बना सकें।
लेख

श्री गौरव शाहू
पीएचडी (समाज कार्य)
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)


