मंत्र विप्लव: नेशनलिज़्म बनाम राष्ट्रत्व
जब ब्रिटिश भारत आए तो वे प्रोटेस्टेंट चर्च द्वारा निर्देशित थे। प्रोटेस्टेंट दिखने में नरम, परंतु एक ही थैली के चट्टे-बट्टे थे।
Total Views |
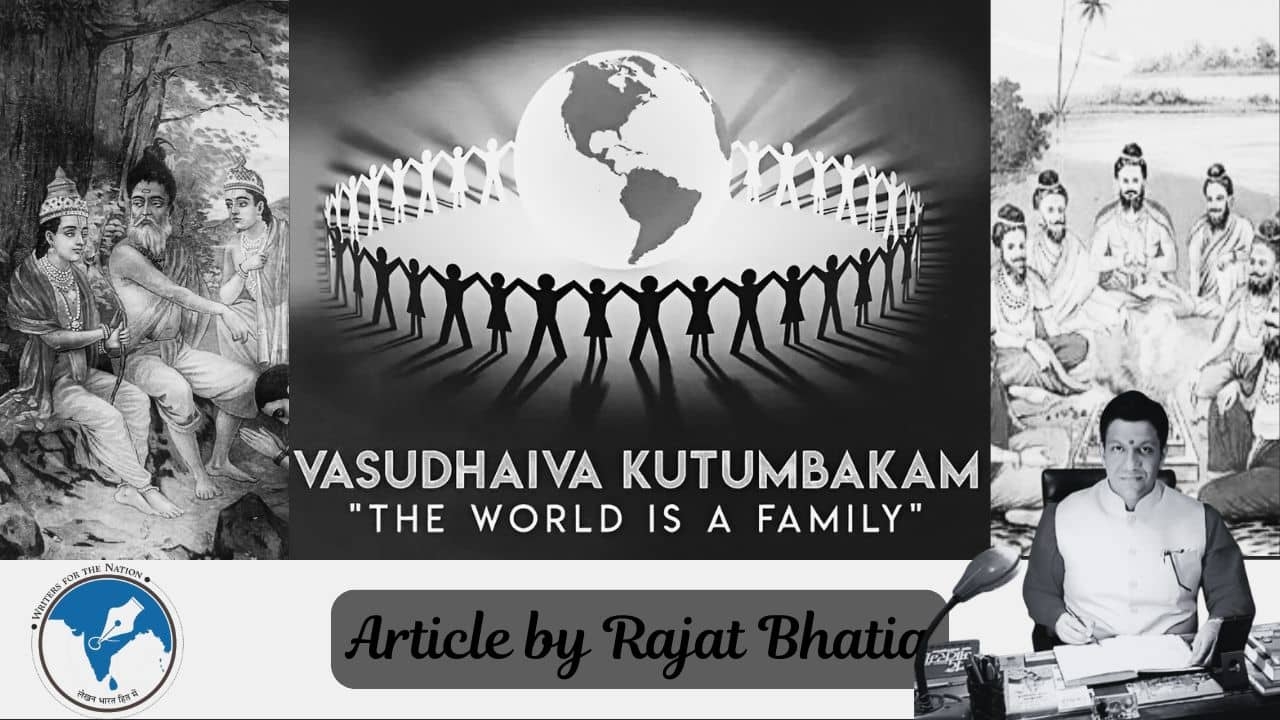
मानवता के इतिहास में विश्व को चरमोत्कर्ष का अहसास करवाने वाली एकमात्र संस्कृति भारतीय संस्कृति है, जिसने विभिन्न कालखंडों में विश्व को शांति, समरसता और सद्भाव का ज्ञान देकर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' एवं 'वैश्विक बंधुत्व' जैसी वैदिक विचारधारा को सार्थक कर 'विश्व गुरु' की उपाधि प्राप्त की।
हमारे वेदकालीन पूर्वजों ने सोचा कि यदि मानव को समत्व से समाजत्व की ओर संस्कारित करना है तो वह गुणों के विकास के आधार पर ही संभव है।
भौतिक वासनाओं से प्रेरित विचार मानव को पशुओं की भांति बांधकर रखेंगे। इस विचार का मार्गदर्शन करने वालों को ऋषि कहा गया है। ऋषि वह हैं जो दृष्टा हैं। परिवर्तनीय संसार में अपरिवर्तनीय गुणों की उत्कृष्टता जानने वाले ज्ञानी हैं—ऋषि।

इन्हीं ज्ञानवान, मनोवैज्ञानिक ऋषियों ने राष्ट्र को संगठित करने हेतु धार्मिक आधार पर अनेक उदाहरण दिए। इसलिए उन्होंने वैदिक मंत्रों और श्लोकों में बहुधातु में एकत्व और विभक्त में अविभक्त को अनुकूल करने के संस्कारों को जनसाधारण तक पहुंचाया।
भारत राष्ट्र में अनेक महात्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने राष्ट्र स्थापना हेतु राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनाईं, जिनमें महात्मा विदुर भी एक थे।

महात्मा विदुर ने अपने ग्रंथ 'विदुर नीति' में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर 'मंत्र विप्लव' का सिद्धांत दिया।
इस सिद्धांत का प्रयोग कर विचारों को सुविधाजनक स्वरूप देकर राष्ट्र को किसी भी प्रकार की आपदाओं से बचाया जा सकता है।
जब ब्रिटिश भारत आए तो वे प्रोटेस्टेंट चर्च द्वारा निर्देशित थे। प्रोटेस्टेंट दिखने में नरम, परंतु एक ही थैली के चट्टे-बट्टे थे।
पुर्तगाली (रोमन कैथोलिक) यदि प्रभु श्रीराम पर प्रहार करने वाली ताड़का हैं तो ब्रिटिश (प्रोटेस्टेंट) श्रीकृष्ण को विषपान करवाने वाली पूतना समान हैं। इनका प्रहार मायावी था, परंतु बेहद खतरनाक।
महर्षि विदुर द्वारा दिए गए मंत्र विप्लव सिद्धांत का उपयोग अंग्रेजों ने भारतीय जनता के मन में विकृति उत्पन्न करने के लिए किया, जिससे वे अपना स्वत्व भूलकर पुरुषार्थहीन होकर शून्य हो सकें और सामाजिक स्तर पर ब्रिटिशों की कठपुतली बनकर उनके इशारों पर नाच सकें।
इसी सिद्धांत का प्रयोग कर यूरोपीय देशों में से ब्रिटिश भारत पर शासन करने में सबसे सफल रहे। उनका वैचारिक विकृतिकरण का प्रहार भारतीय समाज में वर्तमान समय तक देखा जा सकता है।
भारत का वेदजन्य राष्ट्र नर केंद्रित न होकर राष्ट्र केंद्रित है। अतः इस प्रकार प्राचीन सभ्यता का साधक सर्वप्रथम मानता है कि यह पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं—"माता भूमिः पुत्रोऽहम् पृथिव्याः।" (अथर्ववेद 12.1.12)
इसी श्लोक के अंतर्गत प्रार्थना स्वर में कहा गया है, "हे मातृभूमि, हम सब आपके शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं। आपके शरीर पर विचरण करते रहते हैं।
पांच प्रकार के जन—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद—सब समान हैं तथा आप ही की संतान हैं।" (अनुवाद—अथर्ववेद 12.1.15)
राष्ट्र और राष्ट्रत्व का नाता वेदकालीन समय से माता-पुत्र का है। वेदकाल से ही भारत में मातृभूमि की संकल्पना उभर पड़ी। मातृत्व की संवेदना सार्वत्रिक है, परंतु पितृत्व की संवेदना नरोत्तम प्राणियों में अदृश्य है।
पितृभूमि की भावना मातृभूमि की तुलना में अस्वाभाविक है। पिता जन्म हेतु है तो माता जन्मदात्री है। जनित का प्रथम संबंध सर्वप्रथम जन्मदात्री से है।
इसी दृष्टि में भारत के मानव ने भारत की भूमि को माता के स्थान पर देखा तो देशप्रेम का विचार मूलतः भारतीय जनमानस में शामिल रहा।
इस अनुसार भारतीय देशप्रेम को अंग्रेजी के 'पैट्रिऑटिज़्म' शब्द में कहना गलत होगा, परंतु 'मैट्रिऑटिज़्म' कहना ठीक होगा। भारत राष्ट्र में देशभक्ति का सीधा संबंध मातृभक्ति से है।
अथर्ववेद के 12वें खंड के प्रथम सूक्त में महर्षि अथर्व कहते हैं—"हे हमारी मातृभूमि! जो हम लोग तुमसे उत्पन्न हुए हैं, वे निरोगी, दीर्घायु, बुद्धिमान, जागृति संपन्न रहें तथा आपके हित के लिए अपने स्वार्थ की बलि देने में सदैव तत्पर रहें तथा सभी प्रकार से आपका हित करने में समर्पित रहें।" (अनुवाद—अथर्ववेद 12.1.62)
वेदमूर्ति पंडित सातवलेकर जी ऋग्वेद की ऋचा (1.188.8) "भारती या सरस्वती, या वो महि देवि तुभ्यम्" का भावार्थ देते हैं कि मातृभूमि, मातृभाषा और मातृसंस्कृति—इन तीनों की उपासना करनी चाहिए।
इन तीनों का सदा सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे सदा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होती हैं। जो इनकी उपासना करता है वह ऐश्वर्यशाली होता है।
सहस्त्र वर्षों से चलते आए भारतीय वैदिक राष्ट्रत्व को यूरोपीय नेशनलिज़्म का सर्वप्रथम अनुभव 1498 में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा निर्देशित वास्को डी गामा के भारत आने के बाद, सेंट जेवियर द्वारा किए गए 'गोवा इनक्विज़िशन' से हुआ।
जहाँ ईसाईयत के नाम पर प्रशासन के साथ मिलकर लगभग 600 मंदिरों को ध्वस्त किया गया। यहाँ तक कि इस्लामी आक्रमणकारियों ने भी इतने छोटे इलाके में इतने मंदिर नहीं गिराए थे। रोमन कैथोलिक चर्च की विचारधारा ने कट्टरवादी स्वरूप से भारत की राष्ट्रीयता पर प्रहार किया।
जब यूरोप से औपनिवेशिक शक्तियां भारत पहुंचीं, तब उनके साथ उनका पश्चिमी नेशनलिज़्म भी भारत आया। उस समय भारत की वेदकालीन राष्ट्रीयता यूरोपीय विचारधारा की नेशनलिज़्म से श्रेष्ठ थी। दोनों का स्वभाव मूलतः भिन्न है, इसलिए दोनों एक-दूसरे के समानार्थी नहीं हो सकते।
हिंदू के मंदिर, ईसाई के गिरजाघर, मुस्लिम के मस्जिद—तीनों उपासना केंद्र हैं, परंतु भाषांतर में समानार्थी नहीं हो सकते क्योंकि इनका मूल स्वभाव भिन्न है।
विश्व में प्रत्येक देश में, प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ वहाँ की पृष्ठभूमि और इतिहास पर निर्भर करता है। भारत का राष्ट्रत्व और पश्चिम का नेशनलिज़्म इसी तरह के दो शब्द हैं।
भारत का राष्ट्रत्व शांतिजन्य, विकासमान है, परंतु पश्चिमी नेशनलिज़्म के विषय में ऐसा कहना कठिन है। ईसाई सर्वेसर्वा पोप महाशय के निरंकुश आग्रह, राजाओं की मनमानी, आपसी स्पर्धा, वैवाहिक संबंध, साम्राज्य के युद्ध, कैथोलिक-प्रोटेस्टेंट झगड़े, इस्लाम के बढ़ते प्रभाव आदि के कारण यूरोप में नेशनलिज़्म का उदय हुआ। कुल मिलाकर नेशनलिज़्म यूरोप की राजनीतिक प्रतिक्रिया का फल था। भारत के राष्ट्रत्व में समानता का भाव, सांस्कृतिक आस्था भी शामिल है, बहुदेवतावादी धार्मिक स्वतंत्रता है, परंतु यूरोप के नेशनलिज़्म में कट्टरवाद, एकेश्वरवाद जैसी रूढ़ीवादी विचारधाराएं हैं।

यूरोपीय विचारधारा की प्रोटेस्टेंट चर्च की आज्ञानुसार ब्रिटिश भारत आए, जो 1757 से 1947 तक भारत में रहे। इस कालखंड को 1757 से 1857 तक तथा 1858 से 1947 तक विभाजित कर सकते हैं।
प्रथम भाग में 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक। इस दौरान पूरा वर्चस्व ईस्ट इंडिया कंपनी का था, जिसने भारत के बंगाल से लेकर पंजाब तक अपना कब्जा स्थापित किया। प्लासी के रक्तपात का साहसी प्रयास पंजाब के अपहरण पर जाकर समाप्त हुआ।
कंपनी की शासन प्रणाली को 'काजू फली तोड़ने' के उदाहरण से समझ सकते हैं—जैसे कच्चा काजू एक-एक कर तोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार कंपनी के कप्तानों ने रणनीति बनाकर भारत के एक-एक राज्य पर कब्जा किया। यह काल कंपनी शासन के ब्रिटिश शासन में स्थापना का काल था।

दूसरा कालखंड है राजा-रानी की अधीनता का। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ही यहाँ अंग्रेजी संसद के अधीन प्रशासन आरंभ हुआ। तब से अंग्रेजी राजा के प्रतिनिधि वायसरॉय यहाँ प्रशासक बनकर आने लगे। मूलतः वायसरॉय का शब्दार्थ उप-राजा होता है।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम संगठित स्वतंत्रता संग्राम कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसी संग्राम के दौरान संपूर्ण भारत ने एक साथ अपनी-अपनी रणनीति अनुसार कंपनी का विरोध किया था।
विनायक दामोदर सावरकर ने 1906 में भारत की राष्ट्रीयता के पुनः प्रवाह के लिए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नीले आसमान में हिंदुओं का भगवा रंग तथा मुसलमानों का हरा रंग एक साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के यूनियन जैक के सामने खड़ा रहा, जिससे कंपनी का राज्य भारत की धरती से अपने पांव उठाने पर मजबूर हो चुका था। परंतु कंपनी ने दीर्घकालीन योजना बनाने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टी को भारत में स्थापित किया गया।
कंपनी शासन के काल में ही अंग्रेजों द्वारा मंत्र विप्लव का बीज बोया गया। उनकी शिक्षा प्रणाली, उनका प्रचार, चर्च के प्रोपेगेंडा आदि के कारण अंग्रेजों को यहाँ देवदूत की तरह स्थापित किया गया। योजनापूर्वक ब्रिटिश शासन की तरफ से दो शब्द प्रचलित हुए—दैवी विधान और गोरे साहब का ऋण भार।
संकेत यह था कि काले नरसमूह की भलाई के लिए ईश्वर की योजना अनुसार गोरे अंग्रेज भारत आए। भारतीय समाज के दिलों में निम्न भाव पैदा किया गया।
इसी अंतर्गत यह नैरेटिव चलाया गया कि भारत एक राष्ट्र नहीं, भारत पृथ्वी का देश नहीं बल्कि सिर्फ एक भूभाग है, यहाँ का गर्म मौसम सबको उदास बनाने वाला है आदि, जो जनसाधारण तक घुसने लगा, जिससे राष्ट्रीय अस्मिता की विस्मृति हुई।
इस मंत्र विप्लव का भरपूर उपयोग ब्रिटिश शासन द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी विषैली नेशनलिज़्म की विचारधारा को भारत की राष्ट्रीयता को खंडित करने हेतु जनसाधारण तक प्रचारित किया।
इसी झूठे प्रचार ज्ञान को नैरेटिव कहा गया क्योंकि उन्होंने 'फूट डालो, राज करो' की नीति पर काम करने के लिए भारतीय समाज में चल रहे वैचारिक मतभेदों को उठाया और उनके बारे में झूठा संदेश बनाकर जनता तक पहुंचाया।
परंतु स्वतंत्रता के अमृत काल में भी ब्रिटिश शासन का काम यहाँ के वामपंथी विचारकों द्वारा किया जा रहा है, जिसका भारत की सत्यनिष्ठा वाले विमर्श से प्रतिउत्तर देना होगा।
लेख
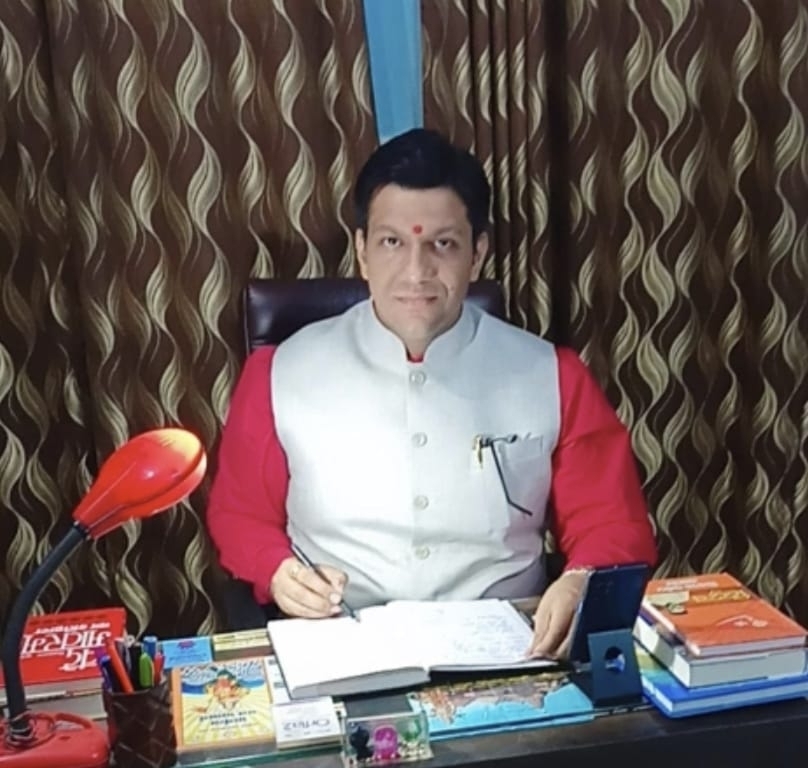
रजत भाटिया
स्तंभकार - Writers For The Nation

